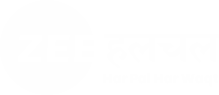रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर के सार्वजनिक बयान ने अंतरराष्ट्रीय हलचल मचा दी है। उन्होंने भारत और चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस से तेल खरीद कर ये देश युद्ध को वित्तीय रूप से समर्थन दे रहे हैं। उनका कड़ा संदेश था—“Your purchases killed…”—जिसका तात्पर्य है कि इन देशों की खरीदारी ने निर्दोषों की जान मारी।
कई अन्य वैश्विक नीतिगत मामलों की तरह, यह भी केवल एक बयान नहीं बल्कि एक गहन विचार-विमर्श की शुरुआत है। इसी कड़ी में पहले भी अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ दोगुना करने का मुद्दा सामने आ चुका है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया था।
अमेरिकी सीनेटर का आरोप और संदेश
इस बयान में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि भारत और चीन की ऊर्जा नीति रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उनका कहना था कि जब तक रूस को तेल और गैस से आमदनी मिलती रहेगी, तब तक वह युद्ध बंद करने के लिए मजबूर नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा खरीदने वाले देश चाहे सीधे युद्ध में शामिल न हों, लेकिन उनकी खरीदारी का पैसा हथियार और मिसाइलों में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए बड़े देश वैश्विक शांति से समझौता कर रहे हैं?
रूस-यूक्रेन युद्ध और तेल व्यापार का प्रभाव
रूस पर पहले से ही पश्चिमी देशों ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। बावजूद इसके, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढही नहीं है क्योंकि तेल और गैस का निर्यात उसके लिए लाइफलाइन बना हुआ है।
भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। इससे रूस को लगातार अरबों डॉलर की आमदनी हो रही है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों का आरोप है कि युद्ध की आग को बुझाने के बजाय एशियाई देशों की नीतियां उसमें और ईंधन डाल रही हैं।
‘Paying the price for supporting Putin’: US Senator Lindsey Graham once again warns India over Russian oil amid rising trade tensions with America
News18’s @siddhantvm with details @DhantaNews | #IndiaUSTrade #IndiaUSRelations pic.twitter.com/e94KVM2mnE
— News18 (@CNNnews18) August 29, 2025
भारत की ऊर्जा रणनीति और दृष्टिकोण
भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। बढ़ती जनसंख्या और उद्योगों की ज़रूरतों के कारण भारत को बड़े पैमाने पर तेल आयात करना पड़ता है।
रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को आर्थिक राहत मिली है। इससे महंगाई पर काबू रखने और घरेलू बाजार को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। भारतीय कूटनीतिक हलकों का मानना है कि “राष्ट्रीय हित किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव से ऊपर हैं।”
चीन का पक्ष और तेल पर निर्भरता
भारत के साथ-साथ चीन भी ऊर्जा के लिए बाहरी बाजारों पर निर्भर है। चीन ने रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध और मजबूत किए हैं। सस्ता और लगातार उपलब्ध रहने वाला तेल उसकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।
हालांकि, चीन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि उसकी नीतियों से रूस को वैश्विक प्रतिबंधों का उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। लेकिन बीजिंग ने अब तक इस मसले पर सीधा कोई बयान देने से परहेज किया है।
अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया
अमेरिका और यूरोप लगातार यही संदेश देते आ रहे हैं कि रूस से ऊर्जा खरीदना युद्ध को लंबा खींचने जैसा है। पश्चिमी देशों की कोशिश है कि रूस की अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह सैन्य कार्रवाई जारी न रख सके।
यही कारण है कि जब भी भारत या चीन जैसे देश रूस से तेल आयात बढ़ाते हैं, तो पश्चिमी नेताओं की प्रतिक्रिया कड़ी होती है। उनका मानना है कि अगर बड़े देश मिलकर रूस पर आर्थिक दबाव डालें तो युद्ध को खत्म करने की संभावना बढ़ सकती है।
भारत-चीन की स्थिति पर वैश्विक विश्लेषण
अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि भारत और चीन दोनों ही अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं। जहां भारत लोकतांत्रिक ढांचे के तहत जनता और उद्योगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दे रहा है, वहीं चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन यह भी सच है कि इन दोनों देशों के फैसलों का असर वैश्विक राजनीति और युद्ध की दिशा पर पड़ रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारत-चीन पर दबाव और बढ़ सकता है।
भारत की घरेलू राजनीति और कूटनीति पर असर
भारत की ऊर्जा नीति केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी है। विपक्ष कई बार सवाल उठाता है कि क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने के पीछे केवल आर्थिक लाभ है या फिर यह रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है।
दूसरी ओर, सरकार का स्पष्ट मत है कि भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही फैसले करेगा। यही कारण है कि अमेरिका के कई बयानों के बावजूद भारत ने अपना रुख नहीं बदला है।
भविष्य की संभावनाएँ और परिदृश्य
अगर भारत और चीन रूस से तेल खरीद जारी रखते हैं, तो रूस को आर्थिक रूप से और लंबे समय तक मजबूती मिलती रहेगी। इससे युद्ध लंबा खिंच सकता है।
वहीं, अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता है और ये दोनों देश रूस से दूरी बनाते हैं, तो वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में उथल-पुथल मच सकती है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
अमेरिकी सीनेटर का यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की जटिलता को उजागर करता है। एक ओर युद्ध की विभीषिका है, दूसरी ओर ऊर्जा की अनिवार्यता।
भारत और चीन के सामने दोहरी चुनौती है – अपने नागरिकों की ज़रूरतें पूरी करना और साथ ही वैश्विक शांति की जिम्मेदारी निभाना।
👉 अब सवाल यह है कि भारत को किस राह पर चलना चाहिए – क्या राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए नीति बदलनी चाहिए?
पाठकों, इस पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।