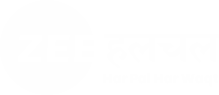अमेरिकी राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब अदालत ने US Reciprocal Tariffs को गैर-कानूनी करार दिया। लेकिन फैसला लागू होने से ठीक पहले ट्रम्प कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इसे देरी कराने की कोशिश की। उनका कहना था कि यह निर्णय अचानक लागू हुआ तो अमेरिका को राजनयिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
यह कदम केवल कानूनी बहस नहीं था, बल्कि इसका असर सीधा वैश्विक व्यापार, अमेरिकी उद्योगों और अन्य देशों के साथ संबंधों पर पड़ने वाला था। यही कारण है कि मामला केवल अदालत और सरकार तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की सुर्खियों तक फैल गया।
Reciprocal Tariffs क्या हैं और क्यों लगाए गए थे
Reciprocal tariffs का सीधा अर्थ है—अगर कोई देश अमेरिका पर ऊँचे शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उसी अनुपात में जवाब देगा। ट्रम्प प्रशासन ने इसे इस तर्क के साथ लागू किया कि इससे अमेरिकी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में फायदा मिलेगा और व्यापार घाटा कम होगा।
दरअसल, अमेरिका का कई देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। इस घाटे को कम करने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अचानक यह कदम उठाया गया।
लेकिन सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार है? प्रशासन ने इसे आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के अंतर्गत लागू किया, जबकि आलोचकों का कहना था कि टैरिफ लगाना संसद यानी कांग्रेस का अधिकार है।
Trump cabinet officials told a federal appeals court that ruling the president’s global tariffs illegal would seriously harm US foreign policy, with Treasury Secretary Scott Bessent warning of “dangerous diplomatic embarrassment.”
The administration filed statements by Bessent,…— Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) August 30, 2025
अदालत का निर्णय – क्यों कहा गया अवैध
अदालत ने गहन सुनवाई के बाद कहा कि कानून में राष्ट्रपति को इतने व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपातकालीन शक्तियाँ केवल सीमित परिस्थितियों के लिए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल एक व्यापक व्यापार नीति बनाने के लिए नहीं किया जा सकता।
निर्णय में यह साफ कहा गया कि व्यापार नीति तय करना और टैरिफ लगाना विधायी शाखा यानी कांग्रेस का अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रपति इस तरह से फैसले लेने लगेंगे तो शक्ति संतुलन का तंत्र बिगड़ जाएगा।
कैबिनेट की देरी कराने की रणनीति
निर्णय आने से ठीक पहले ट्रम्प कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य सक्रिय हो गए। उनका तर्क था कि यदि अदालत का आदेश तुरंत लागू हुआ तो इससे अमेरिका की विदेश नीति को झटका लगेगा।
उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका की छवि एक अस्थिर साझेदार के रूप में बनेगी और कई देशों के साथ पहले से चल रही व्यापारिक वार्ताओं पर असर पड़ेगा। यह भी कहा गया कि निवेशकों और उद्योगों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा, जिससे घरेलू बाजार पर भी बुरा प्रभाव होगा।
सरकारी पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई कि अचानक बदलाव से राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को खतरा हो सकता है। हालांकि अदालत ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना और अपना आदेश जारी रखा।
अंतरराष्ट्रीय असर और आर्थिक परिणाम
इस फैसले का असर न केवल अमेरिका बल्कि उन सभी देशों पर पड़ा जिन पर ये टैरिफ लागू थे। कई देशों ने राहत की सांस ली क्योंकि अब उनके उत्पादों पर भारी शुल्क नहीं लगेगा।
लेकिन अमेरिकी उद्योगों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। जिन कंपनियों ने अपनी उत्पादन योजनाएँ इन टैरिफ दरों को ध्यान में रखकर बनाई थीं, अब उन्हें रणनीति बदलनी होगी।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर साफ दिखाई देगा। अचानक बदलाव से लागत बढ़ सकती है, निवेशक सतर्क हो सकते हैं और बाज़ार में अस्थिरता आ सकती है।
यही कारण है कि इस मामले को कई विशेषज्ञ उसी श्रेणी में रखते हैं जैसे हाल ही में उस समय हुआ जब अमेरिकी सीनेटर ने भारत, चीन और रूस को तेल खरीद पर चेतावनी दी थी। दोनों घटनाएँ दर्शाती हैं कि वैश्विक व्यापारिक फैसलों का असर सीधे देशों के रिश्तों पर पड़ता है।
अमेरिकी राजनीति में बहस
इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे संविधान और लोकतांत्रिक संतुलन की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को बिना अनुमति इतने बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
दूसरी ओर, सत्ता पक्ष के समर्थक इसे कार्यकारी शक्ति का सही इस्तेमाल बता रहे हैं। उनका कहना है कि मजबूत नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए।
चुनावी वर्ष में यह बहस और तेज हो गई है। आने वाले चुनावों में यह विषय निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बनेगा।
विशेषज्ञों की राय और आगे का रास्ता
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और राष्ट्रपति की शक्तियों के बीच स्पष्ट सीमाएँ हैं। भविष्य में किसी भी प्रशासन को इस प्रकार का कदम उठाने से पहले संसद की मंज़ूरी लेनी होगी।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टैरिफ पूरी तरह से हटा दिए गए तो अमेरिका के उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे वैश्विक व्यापार में स्थिरता आएगी।
पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि यह केवल व्यापार नीति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली और शक्ति संतुलन का भी सवाल है।
अब सवाल यह है—
क्या राष्ट्रपति को व्यापार नीति पर इतने व्यापक निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए?
या यह जिम्मेदारी केवल संसद तक सीमित रहनी चाहिए?
👉 इस पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।